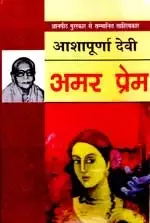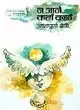|
नारी विमर्श >> अमर प्रेम अमर प्रेमआशापूर्णा देवी
|
204 पाठक हैं |
||||||
नारी के जीवन पर आधारित उपन्यास...
Amar Prem a hindi book by Ashapurna Devi - अमर प्रेम - आशापूर्णा देवी
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित बंगला की शीर्षस्थ लेखिका आशापूर्णा देवी का एक नया उपन्यास।
आशापूर्णा देवी का लेखन उनका निजी संसार नही है। वह हमारे आस-पास फैले संसार का विस्तार मात्र हैं।
इनके उपन्यास मूलतः नारी केन्द्रित होते हैं सृजन की श्रेष्ठ सहभागी होते हुए भी भारतीय समाज में नारी का पुरूष के समान मूल्याकंन नहीं ?
पुरूष की बड़ी-सी कमजोरी पर समाज में कोई हलचल नहीं, लेकिन नारी की थोड़ी-सी चूक उसके जीवन को रसातल में डाल देती है। यह है एक असहाय विडम्बना !
बंकिम, रवीन्द्र, शरत् के पश्चात् आशापूर्णा देवी हिन्दी भाषी अंचल में एक सुपरिचित नाम हैं- जिनकी हर कृति एक नई अपेक्षा के साथ पढ़ी जाती है।
आशापूर्णा देवी का लेखन उनका निजी संसार नही है। वह हमारे आस-पास फैले संसार का विस्तार मात्र हैं।
इनके उपन्यास मूलतः नारी केन्द्रित होते हैं सृजन की श्रेष्ठ सहभागी होते हुए भी भारतीय समाज में नारी का पुरूष के समान मूल्याकंन नहीं ?
पुरूष की बड़ी-सी कमजोरी पर समाज में कोई हलचल नहीं, लेकिन नारी की थोड़ी-सी चूक उसके जीवन को रसातल में डाल देती है। यह है एक असहाय विडम्बना !
बंकिम, रवीन्द्र, शरत् के पश्चात् आशापूर्णा देवी हिन्दी भाषी अंचल में एक सुपरिचित नाम हैं- जिनकी हर कृति एक नई अपेक्षा के साथ पढ़ी जाती है।
निवेदिता
बांग्ला लेखिका आशापूर्णा देवी का जन्म 8 जनवरी, सन् 1910 को हुआ। पिछले वर्षों में अपनी 175 औपन्यासिक तथा कथाकृतियों के माध्यम से अपने मानव स्वभाव के अनेक पक्षों को उजागर किया है। बंकिम, रवीन्द्र और शरतचन्द्र के पश्चात आशापूर्णा ही ऐसा सुपरिचित नाम है, जिसकी प्रत्येक कृति पिछली आधी शताब्दी से बांग्ला और अन्य भाषाओं में एक नई अपेक्षा से पढ़ी जाती रही है।
कलकत्ता से दिल्ली आया था कि कुछ दिन यहाँ अपने बेटे के पास आराम करूंगा, दिल्ली में आने के बाद एक दिन वैसे ही मन में आया कि जाकर अपने उन प्रकाशक मित्रों से मिलूं जो मुझे इस उमर में भी आराम नहीं करने देते। जैसे ही पहुंचा तो मेरे हाथ में थमा दिया गया यह उपन्यास।
आशापूर्णा का है इसी लिए जल्दी ही प्रारम्भ कर दिया। प्रेम की रीति कितनी पुरानी है पहली पंक्ति से घटना का आरम्भ होता है प्रेमी हृदय अपने लिए नहीं बल्कि अपने मन के मीत के लिए क्या कुछ नहीं करते कथासार मात्र यह है।
परंतु प्रेम यदि प्रेम है तो उसके शत्रु भी अनेक हैं।
अहमिका ही इसकी सदा की शत्रु है।
कभी समाज की अहमिका कभी अभिभावकों की अहमिका, कभी केवल अपनी, अपने मन की अहमिका यह प्रेम को हरगिज अपनी महिमा में विकसित नहीं होने देती ! ध्वंस किये देती है मगर चीजें तो पलटती हैं परिवर्तन का यह इतिहास ही तो मनुष्य का, जगत का इतिहास है। प्रेम और अहमिका की हार जीत भी क्या एक दिन बदली नहीं जा सकेगी ?
कहानी में नायिका की भूमिका निबाहने वाली सुलता और कथानायक शशांक भी न बदल सका अपने आपको आधुनिक होने का नाटक तो करता है इसके लिए प्रेम विवाह भी करता है परंतु विचारधारा तो पुरानी ही है, घर के प्रति परिवार के प्रति मोह तो होगा ही अतएव जब सुलता अपनी माँ के बहकावे में उसका उसे नया अलग फ्लैट लेने को कहती है तो उसका मन नहीं मानता यहाँ से टकराव के बीज का अंकुरण होता है।
आशापूर्णा भारतीय नारी के आधुनिक होने के नाम पर उच्छृंखलित या पारिवारिक मर्यादाओं की अनदेखी करने का न तो प्रस्ताव रखती है और न ही उसकी ऐसी कोई पैरवी करती हैं जिससे कि अपनी किसी बात को एक जिद्दी दलील के तौर पर उद्धृत किया जाये।
उन्होंने समाज के विभिन्न स्तरों पर ऐसे असंख्य पात्रों की मनोदशाओं का चित्रण किया है जो अबोले हैं, या जो खुद नहीं बोलते—भले ही दूसरे लोग उनके बारे में हजार तरह की बातें करें।
आशापूर्णा समाजशास्त्री, शिक्षा शास्त्री या दार्शनिक की मुद्र ओढ़कर या आधुनिक या प्रगतिशील लेखिका होने का मुखौटा नहीं लगातीं। वे अपनी जमीन और अपने संदर्भ को खूब अच्छी तरह देखती-परखती हैं। आशापूर्णा ने अपने स्त्री पात्रों के अनजाने और अपरिचित कोने से उठाया और सबके बीच और सबके साथ रखा। उसे रसोईघर की दुनिया से बाहर निकालकर वृहत्तर परिवेश देना चाहा। जहाँ नारी का माता-पिता और बेटी वाला शाश्वत रूप सुरक्षित रहा।
अपनी मनमोहिनी शैली में यह कथा आगे बढ़ती है इसका अंत क्या होता है यह यदि बता दूँ तो पढ़ने का आनन्द जाता रहेगा मैंने इसमें प्रादेशिक शब्दों को भी स्थान दिया है उनको अनुवाद नहीं किया है और इस पुस्तक की काव्यमयी धारा को छेड़ा भी नहीं है इसे उसी रूप में आगे बढ़ाया गया है आशा है कि यह उपन्यास अपना यह सन्देश देने में सफल होगा कि प्रेम में ‘‘मैं’’ का स्थान नहीं है यदि ‘‘मैं’’ के स्थान पर हम आ जाए तो जीवन का स्वरूप ही बदल जायेगा।
सुनने में आता है, सुलता की दादी सुखलता की शादी से पहले टोले के एक लड़के से कुछ प्रेम सम्बन्धी घटना घटी थी।
सुखलता की उम्र यद्यपि उस समय दस साल की थी और उस लड़के की साढ़े तेरह, फिर भी वह लड़का दूसरे की बगीची के फूल और पराए पेड़ के बेर चुराने के काम में उसकी जी जान से मदद करता। और सुखलता भी घर से अमचूर चुरा लाकर मित्रों में खैरात बाँटते वक्त उसके प्रति जरा विशेष पक्षपात दिखाती। बालपन के प्रेम के और भी जो ग्रामीण तौर-तरीके उस समय थे, उनका बहुत कुछ ही सिख लिया था उन लोगों ने।
जैसे, टोले में कहीं ‘हरि लूट’ होती तो वह छोरा झपट पड़ता और दोनों हाथों जितने भी बताशे लूट पाता, उसका अधिकांश छिपाकर सुखलता के खोइंचे में डाल देता; और किसी के यहाँ लड़के की ‘अठ कौड़ी’ होती तो सुखलता अपने अँचरे के लावे से बीन-बीन कर गाजा-जलेबी अपने मन के उस मीत की मुट्ठी में खोंस देती। अवश्य औरों से छिपाकर ही।
घर जाने पर मिठाई कम देखकर माँ या दादी अवाक होकर कहती, हाय राम, इतनी ही दूर आने में सारी मिठाइयाँ गड़प गयी ?’ सुखलता निर्विकार-सी कहती—मिठाई मुझे दी ही नहीं। सिर्फ लावा ही दी है।
वे गाल पर हाथ रख लेतीं। कहतीं, लावा ही तो देंगे। जैसे ढपोल हो तुम।
लेकिन अचानक उन सबका भ्रम टूटा।
जानें कैसे तो फूल, बेर और अमचूर वाली घटना कानाफूसी से उनके कानों तक जा पहुँची, और फिर एक दिन घाट जाते वक्त हठात् सुखलता की माँ ने सुना, वह छोरा उनकी बेटी को ‘सुख’ कहकर पुकार रहा है।
‘सुख, सुख, सुख !’
और उस पुकार से उनकी उस ढपोल बिटिया के चेहरे में आँखों में जैसे खुशियाँ छलक रही हैं।
मारे गुस्से के सुखलता की माँ के सिर से पाँव तक आग की लहर-सी दौड़ गयी।
कहा जाता है घर लौटकर माँ ने अपनी कुलबोरन बिटिया को पीट-पीट कर बेरचून बना डाला। तीन दिनों तक उसे कमरे में बन्द रक्खा और तब से जब तक उसका ब्याह नहीं हो गया, बिना पहरे के उसे घर से एक कदम बाहर नहीं निकलने दिया।
अवश्य ही इस ब्याह में भी विलम्ब नहीं हुआ।
सुखलता के बाप-चाचा ने एड़ी चोटी का पसीना एक करके उसके लिए दूल्हा ढूँढ़ा और तीन ही महीने के अन्दर गँठबंधन कराके उसे उसकी ससुराल विदा किया।
अपनी सखियों से सुखलता ने सुना था, उस घटना के बाद लड़के के बड़े चाचा ने भी खड़ाऊँ से पीट-पीट कर लड़के का तख्ता बना छोड़ा था और धमकी दी थी, दुबारा फिर कभी ऐसा किया तो पीठ की खाल उधेड़कर रख दूँगा।
यह सुन कर सूने में रो-रोकर सुखलता ने सर्दी बुला ली थी। अपनी सखी से कहा था, ‘हाय सखी तूने यह क्यों सुनाया मुझे ! यह सुनने से तो मेरा मरना अच्छा था।’
लेकिन दुनिया में ‘अच्छा’ तो ज्यादा होता नहीं है, लिहाजा सुखलता की मौत नहीं हुई, हुई शादी। और जीवन में फिर कभी उससे भेंट नहीं हुई।
वैसे तो ऐसा है कि सुलता के कलकत्ते के इस घर से उसकी दादी सुखलता का मयका महज इक्कीस मील है क्या तो ! और उनका वह ‘पहला प्रेम’ आज भी जीता-जागता मौजूद है।
मगर यह सब बेशक मध्ययुग की घटना है।
आदमी लगभग बर्बर थे उस समय।
लेकिन प्रेम तो हर युग की रीत है।
इसीलिए सुखलता की बेटी चारुलता भी वही काण्ड कर बैठी।
यानी मुहल्ले के एक लड़के के प्रेम में पड़ गयी। शायद ऐसा हो कि चारुलता को यह प्रेम जन्म के सूत्र से ही मिला हो।
चारुलता सुलता की सबसे बड़ी फुआ थी, यानी सुखलता की पहली लड़की, सो उस समय तक बर्बरता सम्पूर्णतया मिटी नहीं थी। इसलिए प्रेम की प्रवणता के प्रति सुविचार नहीं करके चारुलता की भी खासी धुलाई हुई।
लेकिन चूँकि चारुलता की उम्र पन्द्रह पार कर चुकी थी, इसलिए धुलाई शारीरिक नहीं, मानसिक हुई।
और इस काम की अगुआ सुखलता ही हुई।
चारुलता का खिड़की पर खड़ा होना बन्द हुआ, बन्द हुआ छत पर जाना।
नाटक-नाबिल, पढ़ना बन्द हुआ। और उठते-बैठते धिक्कार, लाँछना। कटु, कड़वी, तीती, खट्टी, तरह-तरह के स्वाद के मंतव्यों की बौछार।
और सुखलता ने भी पति की नाक में दम करके छः ही महीने के अन्दर बेटी को ससुराल चलान करने का इंतजाम किया।
चारुलता के किस्से में भी मुहल्ले के उस लड़के को दोनों ओर से बदस्तूर डराया-धमकाया गया। यह भी सुना गया कि वह लड़का बेचारा मन के आवेग से एक दिन हेदुआ तालाब में डूब मरने भी गया था।
क्यों नहीं मरा, यह तो नहीं पता चल सका, लेकिन उन दोनों को शायद उसके बाद, जोरों का जुकाम हुआ था। लड़के को शायद हेदुआ के पानी से और चारुलता को आँखों के पानी से बस खत्म ! इसके बाद चारुलता का उससे प्रेम या प्रेम-पत्र चला था, इसका कोई सबूत नहीं मिला।
भेंट-मुलाकात की भी कहाँ सुनी गयी ! इसलिए समझना चाहिये कि बेचारी चारुलता का अंकुरित प्रेम भी माँ की ही तरह कली में ही सूख गया।
लेकिन सुलता के जमाने में तो वह काल नहीं रहा। आज आदमी सभ्य हुए हैं, सहिष्णु हुए हैं, उनकी बर्बरता जाती रही है।
और नायिकाएँ अब नाबालिग नहीं रहतीं।
प्रेम से पहले वे पढ़ाई की दो-तीन परीक्षाएँ पास कर चुकी होती हैं।
सो सुलता भी जब अपनी दादी सुखलता और फुआ चारुलता की तरह मुहल्ले के नहीं सही, किसी और मुहल्ले के लड़के के प्रेम में पड़ गयी, तो अभिभावकों की मजाल नहीं हुई कि चूँ भी करें।
वे रोज ही यह देखने लगे कि सुलता कालेज से लौटते हुए देर से घर आती है।
पूछा जाता तो डाँट कर जवाब देती, काम था। फिर कोई कुछ भी नहीं कह सकते।
इधर हितू बन्धु खबर दिया करते—सुलता को आउटराम घाट में देखा। साथ में कोई छोकरा था।
खबर देते—सुलता को चेंगवा में बैठकर खाते देखा। कोई लड़का खिला रहा था शायद। गोरा रंग, छरहरा बदन। खूब ‘और लो, और लो’ कर रहा था।
खबर देते-तुम्हारी सुलता को मेट्रो में दाखिल होते देखा। साथ में कोई दोस्त था शायद। देखने में छोकरा अच्छा है।
ये लोग इन खबरों के जहर या जहरीली खबरों को पीकर नीलकंठ बनकर बैठे रहते, सुलता से कुछ कह नहीं सकते।
और दादी अगर कुछ कहने भी जातीं तो दादी की बहू ठंढे धीमे स्वर में हँसती हुई कहतीं—आखिर यह तो मध्ययुग नहीं है कि लड़की के पाँव में जंजीर डाल दें।
अतएव देर से लौटने की उस आदत को और लम्बी करके एकाएक एक दिन जब सुलता अपने उस मित्र के साथ हँसते हुए आकर गुरुजनों को प्रणाम करके खड़ी हो गयी। तो गुरुजनों ने परम प्रशान्त मुख से उस प्रणाम को स्वीकार करके आशीर्वाद दिया।
सिर्फ सुखलता ने भवें सिकोड़ कर कहा था—अरी यह लता अचानक आकर प्रणाम क्यों कर गयी बहू ? और साथ में वह छोकरा ही कौन था ? कभी देखा तो नहीं उसे। एकाएक इतनी भक्ति ?
सुनकर सुखलता की बहू मुँह पर आँचल रखकर हँसी थी !
उसके बाद सुलता के पिता ने जैसा चाहिए, दान-दहेज सजा कर बेटी को आठों अलंकार से मोड़कर बड़े समारोह के साथ कन्या-दान का अभिनय किया। बेटी ने भी खुशी-खुशी दान-सामग्री ले ली और गाँठ जोड़कर दूल्हे के साथ मजे से ससुराल जा पहुँची।
ससुराल में दूध में आलता के पत्थर से लेकर पानी का घड़ा, वरण डाला—किसी नेग की कमी न हुई। खासी दावत भी हुई। किसी बात को लेकर कोई कसर नहीं रही। कसर होती भी तो किस हिम्मत से ? उन्हें, उन तरुणों को भला नाराज करना चाहिए ? वे तो सदा ही ऊपरवालों को झाड़ फेंकने को तैयार रहते हैं। कहीं जरा लापरवाही की, या कि आँखें लाल-पीली कीं कि वे ऊपरवालों को छोड़ कर चल देंगे।
उन्हें रोक रखने की जिम्मेदारी जिनकी है, पकड़े रखने की व्याकुलता जिन्हें है, उन बन्धविहीनों को बाँधने का कौशल उन्हीं को ढूँढ़ निकालना पड़ता है और वस्तु का बंधन ही तो बड़ा बन्धन है। स्नेह से ज्यादा स्नेह का उपहार। प्यार से ज्यादा खुशामद।
प्रौढ़ चारुलता भी हठात् यहाँ-वहाँ फोंस करती करती फिरी—बाप रे, कब किस जनम में मैंने जाने किसी एक लड़के की तरफ ताका था, उसके लिए घर और बाहर कैसी लानत-मलामत हुई मेरी ! कैसे तो ससुरालवालों को भी इसकी भनक मिल गयी और इसके लिए मजाक उड़ाया,. चिकोटी काटी। और अब ? उसी घर में यह हरकत बड़े मजे में चल निकली। सुना क्या था, तो समाज ! समाज ! अब शायद समाज नाम की कोई चीज नहीं रही ?
सुखलता ने कुछ कहा जरूर नहीं, पर कुछ सोचा था क्या ? उन्हें उस खड़ाऊँ से पिटे लड़के की याद आ गयी थी ? या उनका वह सारा कुछ खेल तमाशा हो गया था ?
अवश्य सुखलता और चारुलता इन दोनों में से किसी ने भी ‘प्रेमहीन दाम्पत्य जीवन’ के बोझ से बोझिल होकर कष्ट से काल काटा हो, ऐसी बात नहीं। मजे से, सुख-स्वच्छन्दता के साथ और पति देवता को गाँठ में बाँध करके ठाठ से ही दिन बिताये। तो भी—
लेकिन यह युग उस ‘तो भी’ की परवा नहीं करता। यह युग जिन्दगी के मजे लेना जानता है, सुख को संजोना जानता है।
सो सुलता अपने जीवन की नैया की पतवार अपनी मुट्ठी में लिए बेपरवाह बढ़ने लगी।
ससुराल के लोग तटस्थ रहते—बेटे के प्रेम—विवाहवाली बहू कहीं नाराज न हो जाय। यों शशांक गुस्सैल नहीं है, पर बीबी के डर से गुस्सैल होने में कितनी देर लगती है ?
घर के लोग ज्यादा तीता नहीं खाते, तीन जून उस घर का खाना खाने के बाद ही सुलता ने घोषणा की, रोगियोंवाला यह पथ्य तो मुझ से अब नहीं खाया जायगा।
ये लोग ‘बेड-टी’ नहीं पीते थे। सुलता ने अवाक होकर कहा, ‘बेड-टी’ नहीं पीते हैं, आज भी इस युग में भी ऐसे लोग हैं, यह मैं नहीं जानती थी।
उनके यहाँ अभी भी यह रिवाज था कि पुरुष पहले, स्त्रियाँ पीछे खायेंगी। पुरुष मेज पर और स्त्रियाँ नीचे पीढ़े पर बैठ कर खाना खातीं। घर में लोग बहुत हैं, एक साथ एक मेज पर बन भी नहीं पाता।
इस पुरानी प्रथा को देखकर सुलता ने नाक-भौं टेढ़ी की। कहा, शशांक—नाम से ही मुझे समझना चाहिए था कि यह परिवार कितना पिछड़ा हुआ है।
लेकिन ये बातें आसानी से कही गयीं, खुब गुस्से में नहीं।
कही आसानी से गयीं, मगर ससुराल की अन्य स्त्रियों ने नयी बहू के कहे का महत्व दिया।
रसोई में तीतापन की शुरूआत हुई।
उस रसोई को और लोग आँखें पोंछते हुए ‘सू-सू’ करके खाते, सुलता हँसती हुई स्वाद ले-लेकर खाती।
छोटी ननद शकुन्तला ने भी अब तो बेड-टी चालू कर दी और भैया-भाभी के साथ प्रसाद पाने की आदत डाल ली।
घरवालों ने एक अलग मेज ही खरीद ली, जिस पर सुलता और शशांक आमने-सामने बैठ कर खा सकें।
इस मामले में शशांक ने बेशक जरा किन्तु-परन्तु किया था, किन्तु उस किन्तु-परन्तु को उड़ जाने में देर न लगी। शशांक की बड़ी चाची खुद आगे आयीं और बोलीं, हमारा तो अब इस ढाँचे में नहीं चलने का भैया, मगर तुम लोग क्यों नहीं करोगे ? जिस युग का जो धर्म। तुम्हारे समय का धर्म जो कहता है, जो सिखाता है, तुम वही सुनोगे, वही सीखोगे।
शशांक ने सुर खुजाते हुए कहा, मैं तो इसलिए साढ़े नौ बजे खा लेता हूँ कि काम का तकाजा है। उसको इस समय खाने की क्या पड़ी है ?
‘तेरे साथ खाना ही जरूरत है’—यह कहकर बड़ी चाची मुस्कुराती हुई चली गयीं।
वही मुख्य हैं। उनके ऊपर और किसी की नहीं चलती। प्रतिवाद का प्रश्न भी नहीं।
शशांक ने स्त्री से ही कहने की सोची।
लेकिन आमने-सामने खाने बैठा, तो नजर के सामने उस के सिंगार से आरक्तिम चेहरे को देखकर कुछ कह सकना संभव न लगा।
लाचार जरा घुमाकर बोला।
कहा, ‘‘तुम इसी वक्त खा रही हो, दोपहर को फिर भूख लग जायगी तुम्हें।’’
सुलता ने चेहरे और आँखों में चमक-सी चमका कर कहा, ‘‘दोपहर को वकुलबगान में माँ के पास खाऊँगी।’’
‘‘वकुलबगान में ?’’
माँ के पास ! शशांक को तो यह मालूम न था।
शशांक ने अवाक् होकर कहा, आज शायद जाने को कहा है ?
सुलता दमक कर बोली—जाने को न कहें तो अपने घर नहीं जाना चाहिए ? आज ही क्यों, मैं तो रोज जाती हूँ अपने घर।
‘अपने घर’—यह बात शशांक को खट् से लगी। और फिर यह खबर शशांक के लिए बिलकुल नयी थी, अनसोची। उसे सुलता के रोज मायके जाने के बारे में मालूम नहीं था।
यह वह पिछला जमाना नहीं कि माँ-बहन बहू के नाम से चुगली खायेंगी। बल्कि शशांक के कानों पड़ने से वह कहीं असन्तुष्ट हो और उसी से अनर्थ हो जाय, इस डर से उन लोगों ने यह बात छिपा ही रखी थी।
सुलता ने भी जताने की जरूरत नहीं समझी। ऐसी जरूरी बात भी क्या है !
बहू के रोज-रोज यों मायके जाने की बात को लेकर ससुर और बड़े चाचा-ससुर शुरू में हाँ-हाँ कर उठे थे—सास और बड़ी चाची—सास ने झाँ-झाँ करके उसे दबा दिया।
बोलीं, ‘‘तुम लोग मर्द सूरत हो, तुम्हें इन बातों से क्या ! जाती है तो इसमें तुम्हारा क्या नुकसान होता है ?’’
‘‘नुकसान नहीं होता है ? काफी नुकसान होता है। मानहानि होती है। घर की बहू रोज बाप के यहाँ जाकर खायेगी, यह क्या ! लगता है, यहाँ खाने को नहीं मिलता।’’
‘अहा, वह माँ की गोद की लड़की है। रसोई बन चुकने पर माँ का जी कैसा तो करता है-।’
‘त्रिभुवन में और कहीं गोद की लड़की नहीं देखी है ?’—बड़े बाबू हुँकार कर उठने को थे। बड़ी बहू हँसी। हँस कर उन्हें दबाया।
‘देखी क्यों नहीं है ? मैं खुद क्या हूँ ? यहाँ की मैं बड़ी बहू हूँ तो क्या ! मगर उस तुलना से लाभ क्या है ? अपना युग तो नहीं रहा।
नहीं, वह युग नहीं रहा।
इसीलिए कोई मानना नहीं चाहता।
लिहाजा ये दोनों प्रौढ़ भाई बाहर के कमरे में शतरंज बिछा कर विरस-से बैठ जाते और आड़ी निगाहों से ताक-ताक कर देखा करते कि भरी दोपहरी में बहू पीठ का आँचल उड़ाते हुए, हाथ के बटुए को हिलाते हुए चली जा रही है।
बड़े भाई भवें सिकोड़ कर कहते—घर में दो-दो गाड़ियाँ हैं, और बहू धूप में बस-ट्राम से....।
छोटे बाबू ने कहा, ‘इस वक्त तो लेकिन एक भी गाड़ी यहाँ रहती नहीं है भैया।’
‘नहीं रहती है, तो रखनी पड़ेगी। शशा या पोलू को पहुँचाकर एक गाड़ी लौट आयेगी।
शशा यानी शशांक, बड़े बाबू का इकलौता बेटा। पौलू अर्थात् प्रफुल्ल। छोटे बाबू का बड़ा बेटा।
दोनों ही अच्छा काम करते हैं और गाड़ी रखते हैं।
छोटे बाबू बोले, ‘उनका तो चक्कर मारने का काम है। असुविधा नहीं होगी ?’
‘हो भी तो कोई उपाय नहीं। प्रेस्टीज नाम की चीज है, यह तो मानते हो ? बहू अगर यों घूमा करे तो प्रेस्टीज रहेगी ?
बात तो सही है।
प्रेस्टीज का कानून बड़ा कड़ा है।
उसके एक पल में रसातल जाने का डर है। उसके आगे हाथ-पाँव बँधे हैं। सो, दूसरे दिन से रोज दोपहर में बहू को गाड़ी से मायके पहुँचाने की व्यवस्था की गयी।
दस बजते-बजते तली हुई गरम-गरम मछली, उबला अण्डा, मक्खन और दही के साथ चावल खाकर सुलता पति के साथ-साथ घूमा करती, जब तक कि वह घर से चला नहीं जाता। पति चला जाता तो इस-उस कमरे का चक्कर काटती, कहीं कुछ गपशप, कहीं कुछ काम।
काम का मतलब किसी का थोड़ा –बहुत कुछ सी-सवा देना, किसी चचेरे ननद-देवर को कुछ पढ़ा देना या कमरे को थोड़ा सजा-सवाँर देना।
यह सब सुलता कर दिया करती।
मगर मर्जी पर।
ऐसा भी हुआ है, जैसे शशांक गया, उसका जी बड़ा खराब हो गया, फिर कुछ भी अच्छा न लगा, कमरे में जाकर पड़ रही, या कि अनमनी-सी घण्टों बरामदे पर खड़ी रही। या फिर तुरत पति को टेलीफोन करने बैठ गयी।
एक-डेढ़ बजे गाड़ी आती। हलका-सा सिंगार करके तब निकल पड़ती। लेकिन असभ्य नहीं है वह, अभद्र नहीं है। जाते वक्त सासों से कह जाती, ‘जा रही हूँ माँ, जा रही हूँ बड़ी माँ, जा रही हूँ चाची।’
वह चली जाती तो सासें विगलित चित्त से आपस में कहतीं ‘और जो हो चाहे, तहजीब है।’
वास्तव में तहजीब है, यही होना क्या कम है ? गुरुजनों के लिए यही पाना क्या कुछ कम है ? खास करके बेटे के लव-मैरिजवाली बहू से !
देख-सुन कर लायी गयी बहू को मन के माफिक, घर के अनुकूल बना लेने की दुरूह चेष्टा ऊपरवाले को बड़ी जिल्लत झेलनी पड़ती है। बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है।
लेकिन जो बलपूर्वक अपने अधिकार से आयी है ? न, उस अनिवार्य सम्पर्क में किसी कोशिश का सवाल ही नहीं उठता।
वह अगर घर के सबसे कीमती रतन को लेकर घर से चली न जाय, मिहरबनी करके ससुराल को कृतार्थ करे, तो अभिभावक गण इससे धन्य हो जाते हैं।
लिहाजा यह कहा जा सकता है कि सुलता ने इन लोगों को धन्य किया है। और फिर यदि तहजीब है, तो कहिये कि कृत-कृतार्थ कर रही है।
कलकत्ता से दिल्ली आया था कि कुछ दिन यहाँ अपने बेटे के पास आराम करूंगा, दिल्ली में आने के बाद एक दिन वैसे ही मन में आया कि जाकर अपने उन प्रकाशक मित्रों से मिलूं जो मुझे इस उमर में भी आराम नहीं करने देते। जैसे ही पहुंचा तो मेरे हाथ में थमा दिया गया यह उपन्यास।
आशापूर्णा का है इसी लिए जल्दी ही प्रारम्भ कर दिया। प्रेम की रीति कितनी पुरानी है पहली पंक्ति से घटना का आरम्भ होता है प्रेमी हृदय अपने लिए नहीं बल्कि अपने मन के मीत के लिए क्या कुछ नहीं करते कथासार मात्र यह है।
परंतु प्रेम यदि प्रेम है तो उसके शत्रु भी अनेक हैं।
अहमिका ही इसकी सदा की शत्रु है।
कभी समाज की अहमिका कभी अभिभावकों की अहमिका, कभी केवल अपनी, अपने मन की अहमिका यह प्रेम को हरगिज अपनी महिमा में विकसित नहीं होने देती ! ध्वंस किये देती है मगर चीजें तो पलटती हैं परिवर्तन का यह इतिहास ही तो मनुष्य का, जगत का इतिहास है। प्रेम और अहमिका की हार जीत भी क्या एक दिन बदली नहीं जा सकेगी ?
कहानी में नायिका की भूमिका निबाहने वाली सुलता और कथानायक शशांक भी न बदल सका अपने आपको आधुनिक होने का नाटक तो करता है इसके लिए प्रेम विवाह भी करता है परंतु विचारधारा तो पुरानी ही है, घर के प्रति परिवार के प्रति मोह तो होगा ही अतएव जब सुलता अपनी माँ के बहकावे में उसका उसे नया अलग फ्लैट लेने को कहती है तो उसका मन नहीं मानता यहाँ से टकराव के बीज का अंकुरण होता है।
आशापूर्णा भारतीय नारी के आधुनिक होने के नाम पर उच्छृंखलित या पारिवारिक मर्यादाओं की अनदेखी करने का न तो प्रस्ताव रखती है और न ही उसकी ऐसी कोई पैरवी करती हैं जिससे कि अपनी किसी बात को एक जिद्दी दलील के तौर पर उद्धृत किया जाये।
उन्होंने समाज के विभिन्न स्तरों पर ऐसे असंख्य पात्रों की मनोदशाओं का चित्रण किया है जो अबोले हैं, या जो खुद नहीं बोलते—भले ही दूसरे लोग उनके बारे में हजार तरह की बातें करें।
आशापूर्णा समाजशास्त्री, शिक्षा शास्त्री या दार्शनिक की मुद्र ओढ़कर या आधुनिक या प्रगतिशील लेखिका होने का मुखौटा नहीं लगातीं। वे अपनी जमीन और अपने संदर्भ को खूब अच्छी तरह देखती-परखती हैं। आशापूर्णा ने अपने स्त्री पात्रों के अनजाने और अपरिचित कोने से उठाया और सबके बीच और सबके साथ रखा। उसे रसोईघर की दुनिया से बाहर निकालकर वृहत्तर परिवेश देना चाहा। जहाँ नारी का माता-पिता और बेटी वाला शाश्वत रूप सुरक्षित रहा।
अपनी मनमोहिनी शैली में यह कथा आगे बढ़ती है इसका अंत क्या होता है यह यदि बता दूँ तो पढ़ने का आनन्द जाता रहेगा मैंने इसमें प्रादेशिक शब्दों को भी स्थान दिया है उनको अनुवाद नहीं किया है और इस पुस्तक की काव्यमयी धारा को छेड़ा भी नहीं है इसे उसी रूप में आगे बढ़ाया गया है आशा है कि यह उपन्यास अपना यह सन्देश देने में सफल होगा कि प्रेम में ‘‘मैं’’ का स्थान नहीं है यदि ‘‘मैं’’ के स्थान पर हम आ जाए तो जीवन का स्वरूप ही बदल जायेगा।
सुनने में आता है, सुलता की दादी सुखलता की शादी से पहले टोले के एक लड़के से कुछ प्रेम सम्बन्धी घटना घटी थी।
सुखलता की उम्र यद्यपि उस समय दस साल की थी और उस लड़के की साढ़े तेरह, फिर भी वह लड़का दूसरे की बगीची के फूल और पराए पेड़ के बेर चुराने के काम में उसकी जी जान से मदद करता। और सुखलता भी घर से अमचूर चुरा लाकर मित्रों में खैरात बाँटते वक्त उसके प्रति जरा विशेष पक्षपात दिखाती। बालपन के प्रेम के और भी जो ग्रामीण तौर-तरीके उस समय थे, उनका बहुत कुछ ही सिख लिया था उन लोगों ने।
जैसे, टोले में कहीं ‘हरि लूट’ होती तो वह छोरा झपट पड़ता और दोनों हाथों जितने भी बताशे लूट पाता, उसका अधिकांश छिपाकर सुखलता के खोइंचे में डाल देता; और किसी के यहाँ लड़के की ‘अठ कौड़ी’ होती तो सुखलता अपने अँचरे के लावे से बीन-बीन कर गाजा-जलेबी अपने मन के उस मीत की मुट्ठी में खोंस देती। अवश्य औरों से छिपाकर ही।
घर जाने पर मिठाई कम देखकर माँ या दादी अवाक होकर कहती, हाय राम, इतनी ही दूर आने में सारी मिठाइयाँ गड़प गयी ?’ सुखलता निर्विकार-सी कहती—मिठाई मुझे दी ही नहीं। सिर्फ लावा ही दी है।
वे गाल पर हाथ रख लेतीं। कहतीं, लावा ही तो देंगे। जैसे ढपोल हो तुम।
लेकिन अचानक उन सबका भ्रम टूटा।
जानें कैसे तो फूल, बेर और अमचूर वाली घटना कानाफूसी से उनके कानों तक जा पहुँची, और फिर एक दिन घाट जाते वक्त हठात् सुखलता की माँ ने सुना, वह छोरा उनकी बेटी को ‘सुख’ कहकर पुकार रहा है।
‘सुख, सुख, सुख !’
और उस पुकार से उनकी उस ढपोल बिटिया के चेहरे में आँखों में जैसे खुशियाँ छलक रही हैं।
मारे गुस्से के सुखलता की माँ के सिर से पाँव तक आग की लहर-सी दौड़ गयी।
कहा जाता है घर लौटकर माँ ने अपनी कुलबोरन बिटिया को पीट-पीट कर बेरचून बना डाला। तीन दिनों तक उसे कमरे में बन्द रक्खा और तब से जब तक उसका ब्याह नहीं हो गया, बिना पहरे के उसे घर से एक कदम बाहर नहीं निकलने दिया।
अवश्य ही इस ब्याह में भी विलम्ब नहीं हुआ।
सुखलता के बाप-चाचा ने एड़ी चोटी का पसीना एक करके उसके लिए दूल्हा ढूँढ़ा और तीन ही महीने के अन्दर गँठबंधन कराके उसे उसकी ससुराल विदा किया।
अपनी सखियों से सुखलता ने सुना था, उस घटना के बाद लड़के के बड़े चाचा ने भी खड़ाऊँ से पीट-पीट कर लड़के का तख्ता बना छोड़ा था और धमकी दी थी, दुबारा फिर कभी ऐसा किया तो पीठ की खाल उधेड़कर रख दूँगा।
यह सुन कर सूने में रो-रोकर सुखलता ने सर्दी बुला ली थी। अपनी सखी से कहा था, ‘हाय सखी तूने यह क्यों सुनाया मुझे ! यह सुनने से तो मेरा मरना अच्छा था।’
लेकिन दुनिया में ‘अच्छा’ तो ज्यादा होता नहीं है, लिहाजा सुखलता की मौत नहीं हुई, हुई शादी। और जीवन में फिर कभी उससे भेंट नहीं हुई।
वैसे तो ऐसा है कि सुलता के कलकत्ते के इस घर से उसकी दादी सुखलता का मयका महज इक्कीस मील है क्या तो ! और उनका वह ‘पहला प्रेम’ आज भी जीता-जागता मौजूद है।
मगर यह सब बेशक मध्ययुग की घटना है।
आदमी लगभग बर्बर थे उस समय।
लेकिन प्रेम तो हर युग की रीत है।
इसीलिए सुखलता की बेटी चारुलता भी वही काण्ड कर बैठी।
यानी मुहल्ले के एक लड़के के प्रेम में पड़ गयी। शायद ऐसा हो कि चारुलता को यह प्रेम जन्म के सूत्र से ही मिला हो।
चारुलता सुलता की सबसे बड़ी फुआ थी, यानी सुखलता की पहली लड़की, सो उस समय तक बर्बरता सम्पूर्णतया मिटी नहीं थी। इसलिए प्रेम की प्रवणता के प्रति सुविचार नहीं करके चारुलता की भी खासी धुलाई हुई।
लेकिन चूँकि चारुलता की उम्र पन्द्रह पार कर चुकी थी, इसलिए धुलाई शारीरिक नहीं, मानसिक हुई।
और इस काम की अगुआ सुखलता ही हुई।
चारुलता का खिड़की पर खड़ा होना बन्द हुआ, बन्द हुआ छत पर जाना।
नाटक-नाबिल, पढ़ना बन्द हुआ। और उठते-बैठते धिक्कार, लाँछना। कटु, कड़वी, तीती, खट्टी, तरह-तरह के स्वाद के मंतव्यों की बौछार।
और सुखलता ने भी पति की नाक में दम करके छः ही महीने के अन्दर बेटी को ससुराल चलान करने का इंतजाम किया।
चारुलता के किस्से में भी मुहल्ले के उस लड़के को दोनों ओर से बदस्तूर डराया-धमकाया गया। यह भी सुना गया कि वह लड़का बेचारा मन के आवेग से एक दिन हेदुआ तालाब में डूब मरने भी गया था।
क्यों नहीं मरा, यह तो नहीं पता चल सका, लेकिन उन दोनों को शायद उसके बाद, जोरों का जुकाम हुआ था। लड़के को शायद हेदुआ के पानी से और चारुलता को आँखों के पानी से बस खत्म ! इसके बाद चारुलता का उससे प्रेम या प्रेम-पत्र चला था, इसका कोई सबूत नहीं मिला।
भेंट-मुलाकात की भी कहाँ सुनी गयी ! इसलिए समझना चाहिये कि बेचारी चारुलता का अंकुरित प्रेम भी माँ की ही तरह कली में ही सूख गया।
लेकिन सुलता के जमाने में तो वह काल नहीं रहा। आज आदमी सभ्य हुए हैं, सहिष्णु हुए हैं, उनकी बर्बरता जाती रही है।
और नायिकाएँ अब नाबालिग नहीं रहतीं।
प्रेम से पहले वे पढ़ाई की दो-तीन परीक्षाएँ पास कर चुकी होती हैं।
सो सुलता भी जब अपनी दादी सुखलता और फुआ चारुलता की तरह मुहल्ले के नहीं सही, किसी और मुहल्ले के लड़के के प्रेम में पड़ गयी, तो अभिभावकों की मजाल नहीं हुई कि चूँ भी करें।
वे रोज ही यह देखने लगे कि सुलता कालेज से लौटते हुए देर से घर आती है।
पूछा जाता तो डाँट कर जवाब देती, काम था। फिर कोई कुछ भी नहीं कह सकते।
इधर हितू बन्धु खबर दिया करते—सुलता को आउटराम घाट में देखा। साथ में कोई छोकरा था।
खबर देते—सुलता को चेंगवा में बैठकर खाते देखा। कोई लड़का खिला रहा था शायद। गोरा रंग, छरहरा बदन। खूब ‘और लो, और लो’ कर रहा था।
खबर देते-तुम्हारी सुलता को मेट्रो में दाखिल होते देखा। साथ में कोई दोस्त था शायद। देखने में छोकरा अच्छा है।
ये लोग इन खबरों के जहर या जहरीली खबरों को पीकर नीलकंठ बनकर बैठे रहते, सुलता से कुछ कह नहीं सकते।
और दादी अगर कुछ कहने भी जातीं तो दादी की बहू ठंढे धीमे स्वर में हँसती हुई कहतीं—आखिर यह तो मध्ययुग नहीं है कि लड़की के पाँव में जंजीर डाल दें।
अतएव देर से लौटने की उस आदत को और लम्बी करके एकाएक एक दिन जब सुलता अपने उस मित्र के साथ हँसते हुए आकर गुरुजनों को प्रणाम करके खड़ी हो गयी। तो गुरुजनों ने परम प्रशान्त मुख से उस प्रणाम को स्वीकार करके आशीर्वाद दिया।
सिर्फ सुखलता ने भवें सिकोड़ कर कहा था—अरी यह लता अचानक आकर प्रणाम क्यों कर गयी बहू ? और साथ में वह छोकरा ही कौन था ? कभी देखा तो नहीं उसे। एकाएक इतनी भक्ति ?
सुनकर सुखलता की बहू मुँह पर आँचल रखकर हँसी थी !
उसके बाद सुलता के पिता ने जैसा चाहिए, दान-दहेज सजा कर बेटी को आठों अलंकार से मोड़कर बड़े समारोह के साथ कन्या-दान का अभिनय किया। बेटी ने भी खुशी-खुशी दान-सामग्री ले ली और गाँठ जोड़कर दूल्हे के साथ मजे से ससुराल जा पहुँची।
ससुराल में दूध में आलता के पत्थर से लेकर पानी का घड़ा, वरण डाला—किसी नेग की कमी न हुई। खासी दावत भी हुई। किसी बात को लेकर कोई कसर नहीं रही। कसर होती भी तो किस हिम्मत से ? उन्हें, उन तरुणों को भला नाराज करना चाहिए ? वे तो सदा ही ऊपरवालों को झाड़ फेंकने को तैयार रहते हैं। कहीं जरा लापरवाही की, या कि आँखें लाल-पीली कीं कि वे ऊपरवालों को छोड़ कर चल देंगे।
उन्हें रोक रखने की जिम्मेदारी जिनकी है, पकड़े रखने की व्याकुलता जिन्हें है, उन बन्धविहीनों को बाँधने का कौशल उन्हीं को ढूँढ़ निकालना पड़ता है और वस्तु का बंधन ही तो बड़ा बन्धन है। स्नेह से ज्यादा स्नेह का उपहार। प्यार से ज्यादा खुशामद।
प्रौढ़ चारुलता भी हठात् यहाँ-वहाँ फोंस करती करती फिरी—बाप रे, कब किस जनम में मैंने जाने किसी एक लड़के की तरफ ताका था, उसके लिए घर और बाहर कैसी लानत-मलामत हुई मेरी ! कैसे तो ससुरालवालों को भी इसकी भनक मिल गयी और इसके लिए मजाक उड़ाया,. चिकोटी काटी। और अब ? उसी घर में यह हरकत बड़े मजे में चल निकली। सुना क्या था, तो समाज ! समाज ! अब शायद समाज नाम की कोई चीज नहीं रही ?
सुखलता ने कुछ कहा जरूर नहीं, पर कुछ सोचा था क्या ? उन्हें उस खड़ाऊँ से पिटे लड़के की याद आ गयी थी ? या उनका वह सारा कुछ खेल तमाशा हो गया था ?
अवश्य सुखलता और चारुलता इन दोनों में से किसी ने भी ‘प्रेमहीन दाम्पत्य जीवन’ के बोझ से बोझिल होकर कष्ट से काल काटा हो, ऐसी बात नहीं। मजे से, सुख-स्वच्छन्दता के साथ और पति देवता को गाँठ में बाँध करके ठाठ से ही दिन बिताये। तो भी—
लेकिन यह युग उस ‘तो भी’ की परवा नहीं करता। यह युग जिन्दगी के मजे लेना जानता है, सुख को संजोना जानता है।
सो सुलता अपने जीवन की नैया की पतवार अपनी मुट्ठी में लिए बेपरवाह बढ़ने लगी।
ससुराल के लोग तटस्थ रहते—बेटे के प्रेम—विवाहवाली बहू कहीं नाराज न हो जाय। यों शशांक गुस्सैल नहीं है, पर बीबी के डर से गुस्सैल होने में कितनी देर लगती है ?
घर के लोग ज्यादा तीता नहीं खाते, तीन जून उस घर का खाना खाने के बाद ही सुलता ने घोषणा की, रोगियोंवाला यह पथ्य तो मुझ से अब नहीं खाया जायगा।
ये लोग ‘बेड-टी’ नहीं पीते थे। सुलता ने अवाक होकर कहा, ‘बेड-टी’ नहीं पीते हैं, आज भी इस युग में भी ऐसे लोग हैं, यह मैं नहीं जानती थी।
उनके यहाँ अभी भी यह रिवाज था कि पुरुष पहले, स्त्रियाँ पीछे खायेंगी। पुरुष मेज पर और स्त्रियाँ नीचे पीढ़े पर बैठ कर खाना खातीं। घर में लोग बहुत हैं, एक साथ एक मेज पर बन भी नहीं पाता।
इस पुरानी प्रथा को देखकर सुलता ने नाक-भौं टेढ़ी की। कहा, शशांक—नाम से ही मुझे समझना चाहिए था कि यह परिवार कितना पिछड़ा हुआ है।
लेकिन ये बातें आसानी से कही गयीं, खुब गुस्से में नहीं।
कही आसानी से गयीं, मगर ससुराल की अन्य स्त्रियों ने नयी बहू के कहे का महत्व दिया।
रसोई में तीतापन की शुरूआत हुई।
उस रसोई को और लोग आँखें पोंछते हुए ‘सू-सू’ करके खाते, सुलता हँसती हुई स्वाद ले-लेकर खाती।
छोटी ननद शकुन्तला ने भी अब तो बेड-टी चालू कर दी और भैया-भाभी के साथ प्रसाद पाने की आदत डाल ली।
घरवालों ने एक अलग मेज ही खरीद ली, जिस पर सुलता और शशांक आमने-सामने बैठ कर खा सकें।
इस मामले में शशांक ने बेशक जरा किन्तु-परन्तु किया था, किन्तु उस किन्तु-परन्तु को उड़ जाने में देर न लगी। शशांक की बड़ी चाची खुद आगे आयीं और बोलीं, हमारा तो अब इस ढाँचे में नहीं चलने का भैया, मगर तुम लोग क्यों नहीं करोगे ? जिस युग का जो धर्म। तुम्हारे समय का धर्म जो कहता है, जो सिखाता है, तुम वही सुनोगे, वही सीखोगे।
शशांक ने सुर खुजाते हुए कहा, मैं तो इसलिए साढ़े नौ बजे खा लेता हूँ कि काम का तकाजा है। उसको इस समय खाने की क्या पड़ी है ?
‘तेरे साथ खाना ही जरूरत है’—यह कहकर बड़ी चाची मुस्कुराती हुई चली गयीं।
वही मुख्य हैं। उनके ऊपर और किसी की नहीं चलती। प्रतिवाद का प्रश्न भी नहीं।
शशांक ने स्त्री से ही कहने की सोची।
लेकिन आमने-सामने खाने बैठा, तो नजर के सामने उस के सिंगार से आरक्तिम चेहरे को देखकर कुछ कह सकना संभव न लगा।
लाचार जरा घुमाकर बोला।
कहा, ‘‘तुम इसी वक्त खा रही हो, दोपहर को फिर भूख लग जायगी तुम्हें।’’
सुलता ने चेहरे और आँखों में चमक-सी चमका कर कहा, ‘‘दोपहर को वकुलबगान में माँ के पास खाऊँगी।’’
‘‘वकुलबगान में ?’’
माँ के पास ! शशांक को तो यह मालूम न था।
शशांक ने अवाक् होकर कहा, आज शायद जाने को कहा है ?
सुलता दमक कर बोली—जाने को न कहें तो अपने घर नहीं जाना चाहिए ? आज ही क्यों, मैं तो रोज जाती हूँ अपने घर।
‘अपने घर’—यह बात शशांक को खट् से लगी। और फिर यह खबर शशांक के लिए बिलकुल नयी थी, अनसोची। उसे सुलता के रोज मायके जाने के बारे में मालूम नहीं था।
यह वह पिछला जमाना नहीं कि माँ-बहन बहू के नाम से चुगली खायेंगी। बल्कि शशांक के कानों पड़ने से वह कहीं असन्तुष्ट हो और उसी से अनर्थ हो जाय, इस डर से उन लोगों ने यह बात छिपा ही रखी थी।
सुलता ने भी जताने की जरूरत नहीं समझी। ऐसी जरूरी बात भी क्या है !
बहू के रोज-रोज यों मायके जाने की बात को लेकर ससुर और बड़े चाचा-ससुर शुरू में हाँ-हाँ कर उठे थे—सास और बड़ी चाची—सास ने झाँ-झाँ करके उसे दबा दिया।
बोलीं, ‘‘तुम लोग मर्द सूरत हो, तुम्हें इन बातों से क्या ! जाती है तो इसमें तुम्हारा क्या नुकसान होता है ?’’
‘‘नुकसान नहीं होता है ? काफी नुकसान होता है। मानहानि होती है। घर की बहू रोज बाप के यहाँ जाकर खायेगी, यह क्या ! लगता है, यहाँ खाने को नहीं मिलता।’’
‘अहा, वह माँ की गोद की लड़की है। रसोई बन चुकने पर माँ का जी कैसा तो करता है-।’
‘त्रिभुवन में और कहीं गोद की लड़की नहीं देखी है ?’—बड़े बाबू हुँकार कर उठने को थे। बड़ी बहू हँसी। हँस कर उन्हें दबाया।
‘देखी क्यों नहीं है ? मैं खुद क्या हूँ ? यहाँ की मैं बड़ी बहू हूँ तो क्या ! मगर उस तुलना से लाभ क्या है ? अपना युग तो नहीं रहा।
नहीं, वह युग नहीं रहा।
इसीलिए कोई मानना नहीं चाहता।
लिहाजा ये दोनों प्रौढ़ भाई बाहर के कमरे में शतरंज बिछा कर विरस-से बैठ जाते और आड़ी निगाहों से ताक-ताक कर देखा करते कि भरी दोपहरी में बहू पीठ का आँचल उड़ाते हुए, हाथ के बटुए को हिलाते हुए चली जा रही है।
बड़े भाई भवें सिकोड़ कर कहते—घर में दो-दो गाड़ियाँ हैं, और बहू धूप में बस-ट्राम से....।
छोटे बाबू ने कहा, ‘इस वक्त तो लेकिन एक भी गाड़ी यहाँ रहती नहीं है भैया।’
‘नहीं रहती है, तो रखनी पड़ेगी। शशा या पोलू को पहुँचाकर एक गाड़ी लौट आयेगी।
शशा यानी शशांक, बड़े बाबू का इकलौता बेटा। पौलू अर्थात् प्रफुल्ल। छोटे बाबू का बड़ा बेटा।
दोनों ही अच्छा काम करते हैं और गाड़ी रखते हैं।
छोटे बाबू बोले, ‘उनका तो चक्कर मारने का काम है। असुविधा नहीं होगी ?’
‘हो भी तो कोई उपाय नहीं। प्रेस्टीज नाम की चीज है, यह तो मानते हो ? बहू अगर यों घूमा करे तो प्रेस्टीज रहेगी ?
बात तो सही है।
प्रेस्टीज का कानून बड़ा कड़ा है।
उसके एक पल में रसातल जाने का डर है। उसके आगे हाथ-पाँव बँधे हैं। सो, दूसरे दिन से रोज दोपहर में बहू को गाड़ी से मायके पहुँचाने की व्यवस्था की गयी।
दस बजते-बजते तली हुई गरम-गरम मछली, उबला अण्डा, मक्खन और दही के साथ चावल खाकर सुलता पति के साथ-साथ घूमा करती, जब तक कि वह घर से चला नहीं जाता। पति चला जाता तो इस-उस कमरे का चक्कर काटती, कहीं कुछ गपशप, कहीं कुछ काम।
काम का मतलब किसी का थोड़ा –बहुत कुछ सी-सवा देना, किसी चचेरे ननद-देवर को कुछ पढ़ा देना या कमरे को थोड़ा सजा-सवाँर देना।
यह सब सुलता कर दिया करती।
मगर मर्जी पर।
ऐसा भी हुआ है, जैसे शशांक गया, उसका जी बड़ा खराब हो गया, फिर कुछ भी अच्छा न लगा, कमरे में जाकर पड़ रही, या कि अनमनी-सी घण्टों बरामदे पर खड़ी रही। या फिर तुरत पति को टेलीफोन करने बैठ गयी।
एक-डेढ़ बजे गाड़ी आती। हलका-सा सिंगार करके तब निकल पड़ती। लेकिन असभ्य नहीं है वह, अभद्र नहीं है। जाते वक्त सासों से कह जाती, ‘जा रही हूँ माँ, जा रही हूँ बड़ी माँ, जा रही हूँ चाची।’
वह चली जाती तो सासें विगलित चित्त से आपस में कहतीं ‘और जो हो चाहे, तहजीब है।’
वास्तव में तहजीब है, यही होना क्या कम है ? गुरुजनों के लिए यही पाना क्या कुछ कम है ? खास करके बेटे के लव-मैरिजवाली बहू से !
देख-सुन कर लायी गयी बहू को मन के माफिक, घर के अनुकूल बना लेने की दुरूह चेष्टा ऊपरवाले को बड़ी जिल्लत झेलनी पड़ती है। बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है।
लेकिन जो बलपूर्वक अपने अधिकार से आयी है ? न, उस अनिवार्य सम्पर्क में किसी कोशिश का सवाल ही नहीं उठता।
वह अगर घर के सबसे कीमती रतन को लेकर घर से चली न जाय, मिहरबनी करके ससुराल को कृतार्थ करे, तो अभिभावक गण इससे धन्य हो जाते हैं।
लिहाजा यह कहा जा सकता है कि सुलता ने इन लोगों को धन्य किया है। और फिर यदि तहजीब है, तो कहिये कि कृत-कृतार्थ कर रही है।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book